रात को जब सब सो जाते हैं तो चाँदनी सबकी आँखों में चाँद पाने का ख्वाब परोस देती है | सुबह उठते ही सब निकल पड़ते हैं अपने हिस्से के के उस चाँद को पाने के लिए | जो चाँद सपनों में आया था उसे पाने में कितनी नींदें खराब करनी पड़ती हैं | कभी चाँद मिल भी जाता है तो पता चलता है .. हरी -भरी धरती कहाँ बुरी थी ? अतीत सी पीछा छुड़ा कर वर्तमान जब भविष्य के लिए खुद को होम रहा होता है तो उसे कहाँ पता होता है वहाँ पहुँचकर इस हिस्से की घास दिखाई देगी |घबराता मन सोचता है कल में आज में या कल में आखिर कहानी है खुशी | पाठकों को अपनी कहानी के माध्यम से इत्ती सी पर असली खुशी का पता दे रही है सुपरिचित लेखिका कल्पना मनोरमा जी की कहानी …..
इत्ती-सी खुशी
घरों की मुंडेरें हों या कॉलोनी के पेड़-पौधे, सभी पर छोटे-छोटे बल्बों की रंगीन लड़ियाँ लगा दी गई थीं । उजाले का मर्म अबोले कहाँ जानते हैं; वे तो उजाले को पाकर खुद उत्स में बदल जाते हैं। चौंधियाती साँझ अपने प्रेमी के साथ पसरने को बेताब थी लेकिन चारों ओर बिजली का रुआब इस क़दर तारी था कि पेड़ों का हरा रंग के साथ धरती का भी रंग खिल उठा था। इस बार दीवाली आने से पहले मेरा भी पता बदल गया था। भले एक कमरे का ही सही अपना घर खरीदकर केतन ने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया था। किराए के सीलन भरे घर से निजात मिल चुकी थी।जिंदगी की भव्यता का छोटा-सा परिचय मिला था।
सातवीं मंजिल पर खड़ी मैं नीचे झाँक-झाँक कर देखे जा रही थी। पार्क का मनभावन दृश्य धूसर हो चुकी मेरी आँखों के लिऐ भोर की ओस जैसा लग रहा था। पलट कर अपने चारों ओर देखा तो जल्दी-जल्दी बालकनी में पड़ीं पुरानी चीज़ों को धकेलकर किनारे कर ढक दिया। दो चार ठीक-ठीक गमलों को थोड़े ऊँचे पर रख दिए ताकि आठवीं मंजिल के घरों से हम अच्छे दिख सकें।अभी मैं पौधों पर जमी मिट्टी साफ कर ही रही थी कि मन फिर से हुआ कि लाओ और देंखें नीचे हो क्या रहा है ? जैसा सोचा वैसा ही किया। देखा, एक महिला सुंदर परिधान में निकली और चट से गाड़ी में बैठकर फ़ुर्र गयी।
ये निश्चित ही कुछ खरीदने जा रही होगी।दीवाली है भई!मैंने मन ही मन स्वयं से कहा। क्या मुझे भी इस धनतेरस कुछ ख़रीदना चाहिए? वैसे तो न जाने कब से जिंदगी की मीनमेख ने धनतेरस को कुछ ख़रिदवाना बंद ही करवा दिया था। पर इस बार क्या सच्ची में कुछ ख़रीद लूँ? एक कटोरदान ही सही जैसा वृंदा मौसी के घर देखा था। मैंने जैसे खुद से ही पूछा और खुद ही उत्तर दे दिया। न न बेटे से इतना ख़र्च करवाने के बाद धनतेरस का शगुन करने के लिए नहीं कहूँगी। कुछ न खरीद पाने के बावजूद भी मन हल्का था। मैं आँखें उठा कर अपने सिर के ऊपर तनी छत को शुक्रिया के साथ निहारा। मैं अपने विचारों में निमग्न बालकनी में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गयी और धीरे-धीरे धनिक बस्ती में शर्मीली शाम का उतरना देखने लगी। मन शांत हुआ तो कान हरकत में आ गए और घर के भीतर हो रही खुरस-फुसर पर केंद्रित हो गए।
“मेट्रो सिटी में रहने के अपने ही दुख होते हैं भाई। यहाँ न चैन से जिया जा सकता है न मरा।”
एक आदमी बोल रहा था। उसको सही ठहराते हुए दूसरे ने अपनी मोटी आवाज़ में कहा,
“तभी तो अक्सर लोग कहते मिल ही जाते हैं कि”बृहस्पतिवार की लोई के लिए गाय नहीं,नवरात्रियों में कन्यायें नहीं और दाता को जल्दी से सच्चे जरूरतमंद नहीं मिलते और यदि मिलते भी हैं, तो जुआरी-शराबी; जिनको कुछ देना मतलब उनके परिवार को विपत्ति में डालना। उनसे तो लोगों को तौबा ही कर लेनी चाहिए।”
“चल छोड़ो यार! आज तो अपनी जमेगी न..?”
दोनों आवाज़ें थमी तो खिखियाकर हँसने की समलित आवाज़ गूँज उठी। झपटकर मैंने अंदर झाँकते हुए बेटे से पूछा।
“ये कौन अजीब-अज़ीब बातें कर रहा है ?” मेरे चेहरे पर डर छितरा चुका था।
“अम्मा! मैं बताना भूल गया था। मुख्य द्वार पर बत्ती वाली बंदनवार लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। वही अपने हेल्पर के साथ आया है ।”
“अच्छा, बड़ी अलग-सी बातें कर रहे हैं दोनों।”
“अम्मा धीरे बोलो प्लीज़ अब आप गलियों वाली बस्ती में नहीं सोसायटी में रह रही हो। वे लोग अपनी बातें कर रहे हैं। सबके जीवन के अपने-अपने प्रसंग होते हैं। चलो तुम्हारे छालों की दवाई दिलवा लाता हूँ । देर होगी तो बाज़ार में ठेलम-ठेल मच जाएगी।” मुझे समझाकर वह तुरंत भीतर की ओर मुड़ गया ।
“अम्मा जल्दी करना…!” उसने फिर कहा।
“हाँ, इन लोगों के जाने के बाद ही न!”
“हाँ जी अम्मा!”
सही तो कहा उसने बाज़ार का दूसरा नाम ठेलम-ठेल ही होता है। लाने को मैं खुद भी दवाई ला सकती थी लेकिन त्योहार के दिनों में बच्चे जितना नज़दीक रहें उतनी ज़्यादा ख़ुशी मिलती है। वैसे देखा जाए तो आजकल के बच्चे नौकरी की चकल्लस में नाक तक डूबे रहते हैं। कब वे अपने साथ बैठें और कब परिवार के? अब देखो न आज मेरा ही घर से निकलने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन शरीर की व्यथा कहाँ समझती है मन के संकल्पों को।
“चलता हूँ सर !” अपनी ऊब-चूब में डूबी में फिर से बालकनी में जा बैठी थी कि अचानक उन दोनों ने जाने की आज्ञा बेटे से माँगी तो मुझे भी छुट्टी मिली।
“चलो अच्छा हुआ जल्दी चले गए। केतन कौन से कपड़े पहनूँ ?”
“अम्मा जो आपको पसंद हों।” बेटे ने कमरे की खिड़की बंद करते हुए कहा ।
“बस दो मिनट का समय दो अभी चलती हूँ।” कहते हुए मैंने अलमारी खोली। एक तोतयी रँग का कुरता मेरे हाथ में आया। उलट-पलटकर देखा और वापस रख दिया।अब इसे बाहर नहीं पहनूँगी। गलियों में रहने की और बात थी और मैंने एक ठीक-ठाक साड़ी निकालकर पहन ली।
घर से निकलते हुए बेटे ने कहा,‘क्या बात है अम्मा? आप किन ख़्यालों में खोई हो? सब ठीक तो है न! छाला ज्यादा दर्द कर रहा है?’
“नहीं,जब उम्र बढ़ने लगती है तो चिंताओं की सूची बनिये के ब्याज जैसी बढ़ने लगती है बेटा! कहना था, लेकिन कुछ ख़ास नहीं, कहकर शांत हो गयी।
दो कदम आगे बढ़ते हुए उसने कहा,”अम्मा! मुझे कुछ गैस्टिक जैसी फ़ील हो रही है, लिफ्ट की जगह सीढियां ले लें?” सोचा बच्चे ने इतने मन से हमारे सीढि़यों वाले जीवन में लिफ्ट को प्रगटाया है, तो क्या हुआ! चलो उसके कहने का मान रख लेती हूँ किन्तु घुटनों ने सिरे से इनकार कर दिया और हम चुपचाप लिफ़्ट से उतर गए।
“सारा दिन कम्प्यूटर से चिपके रहते हो, तो गैस नहीं बनेगी और क्या होगा ? थोड़ा घूम टहल लिया करो!” कह कर उसकी बात न मानने की ग्लानि थोड़ी कम की।
बेटा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मैं उसकी बगल में। हम गेट पर पहुँचे तो सलाम कर गार्ड ने गेट खोल दिया। अब गेट खोलना तो उसकी ड्यूटी बनती थी लेकिन सलाम ठोकने की क्या जरूरत थी ? गाड़ी चल रही थी सो सड़क पर पहुँचते ही रफ़्तार में आ गयी ।
सोचा,जाने दो जिसको जो करना है करे मुझे क्या? लेकिन एक अजीब-सी जिद्द उठी और मैंने बोलना शुरू कर दिया।
“गार्ड से कह देना जिसे पसंद हो उसे वह सलाम किया करे बार-बार लेकिन कम से कम मुझे तो वह न ही करे तो अच्छा होगा। उम्र देखी है उसकी? मेरे पिता के बराबर होगी। और तुम! गाड़ी ज़रा आराम से चलाया करो!” साहब होगे सबके लिए पर मेरे वही केतन हो जो कंधे से लटक-लटक कर टॉफी माँगा करते थे। एक साँस में बहुत कुछ कहते हुए स्टेयरिंग पर हाथ रख मैं ढेर भड़क गयी ।
उसने मुस्कुराकर अपने माथे पर पड़े बालों को सम्हालते हुए कहा। “जब तुम मेरे साथ हो, तो न मुझे कुछ होगा और न ही गाड़ी को। और हाँ,ये मिडिल क्लासियत छोड़ो अम्मा।” कहकर होंठो को गोल-गोल कर सीटी बजाने लगा।आख़िरी वाला वाक्य शायद गार्ड वाली बात के लिए था।
दौड़ती हुई गाड़ी थोड़ी-सी स्लो चलने लगी तो मुझे लगा, मेरे कहने का गाढ़ा असर हुआ है लेकिन मैं गलत थी। गाड़ी लाल बत्ती पर रुकने के लिए स्लो हुई थी और देखते-देखते हम कतारों में आ गये थे। ये नज़ारा कभी टी.वी पर देखा करती थी। आज अपनी गाड़ी में हूँ। सोचते हुए बेटे पर नाज़ हो आया। खिड़की की तरफ़ वाले हैंडिल कोे पकड़ बाँह पर सिर टिका लिया। कोई-कोई बात सार्थक होने में आदमी की तिहाई जिंदगी ले लेती है। सोचते हुए जितना सामने से देख सकती थी देखने लगी। क्योंकि घर से बाहर निकल कर ज़्यादा चकमक करना भद्रता की निशानी नहीं होती। मुझे कई बार समझाया गया था ।
मेरी तन्द्रा खिड़की के काँच पर पड़ने वाली धप-धप से टूटी। देखा एक लड़की मैले-कुचैले कपड़े,उलझे बाल और पपड़ाये होंठ लिए एक मरघिल्ला-सा उघारे बदन बच्चा काँख में दबाये,बार-बार दाँत निकाल शीशे से हाथ लगा-लगाकर माथे से लगाये जा रही थी। मानो कह रही थी “पैयाँ लागूँ…।”
बिना देर किये मैं पर्स से सिक्के वाली थैली निकालने लगी तो बेटे ने आव देखा न ताव मेरे हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और अपनी कसम दे कर बोला।
“प्लीज़ इसको कुछ देने मत लगना।”
“क्यों ?”
“अरे इनका तो धंधा है। ये कोई भिकारी-फिकारी नहीं ।”
उसकी ओर से आया अप्रत्याशित वाक्य सुनकर मैं धक्क से रह गयी। मन ग्लानि से भरने लगा। ख़ुशी छिटकर कहीं छिप गयी। बेटे के ऊपर बहुत क्रोध हो आया। इसको अगर ऐसा बोलना ही था तो तुलसी बाबा को लिखना ही नहीं चाहिए था।
‘तुलसी पंछिन के पिये,घटे न सरिता नीर। धरम करें धन न घटे,जो सहाय रघुबीर ।‘
अपनी कमीबेसी के बावजूद भी जब से याद सम्हाली थी दोहे के इसी मर्म के सहारे अपने जीवन की ऊँची-नीची पगडंडियों पर चलती आ रही थी। माँ ने भी तो बचपन में यही सिखाया था़ कि माँगने वालों के हाथ हज़ार बार मरकर फैलते हैं। जितना हो सके खाली न लौटने देना। ये मेरा बच्चा है? इतना कम भी नहीं कमाता है और नियति देखो इसकी! मन विक्षोभ और क्रोध से भरने लगा था। अपनी बनाईं परम्पराएँ जब अपने ही तोड़ते हैं तो आवाज़ नहीं आती लेकिन दिल जार-जार रो पड़ता है।किसी की रुपया-कौड़ी से मदद कर उसके दर्द में सहभागी होना क्या गलत है ? मेरा मन चोटिल हो गया था सो अपने आप रुख बदल गया। मेरी बात का वह उत्तर देता तब तक लाइट ग्रीन हो चुकी थी इसलिए गाड़ी फिर से अपनी लय में आ गयी।
“हो गयी न ! तुम्हारे मन की।” सिर झटककर मैं बाहर की ओर देखने लगी।
अपनी लेन लेते हुए उसने मेरा सारा गुस्सा एक तरफ झाड़कर स्नेह से अपना हाथ मेरे घुटने पर रख दिया। मैंने उसको झटका तो नहीं। सोचा सयाना हो गया है लेकिन धीरे से नीचे सरका दिया।
“अम्मा तुम उसी बात को क्यों पकड़े बैठी हो। थोड़ा प्रेक्टिकल बनना सीखो।” उसकी इस बात पर कुछ नहीं बल्कि बरस पड़ना था मुझे। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली लेकिन उसने बोलना जारी रखा।
“अम्मा तुम नहीं जानती हो इस ‘मेट्रो सिटी के तामझाम। यहाँ की संस्कृति बड़ी निराली और नीरस है ।”
“तो, रहना तो हमें इंसान बनकर ही है न! या जानवर बन जाएँ?” मैंने अपना गुस्सा पीते हुए कहा तो मुझे अपने कान की लवें गर्म होती सी लगीं।b
“बराबर बोला आपने लेकिन यदि हम भिखारियों की बात करें तो ये लोग जो भी भीख माँगते हैं, ‘डायरेक्ट’ उनकी ‘पॉकेट’ में कुछ भी नहीं जाता।”
“तो ?”
“अम्मा! यहाँ हर एक भिखारी के लिए अलग-अलग चौराहा एलॉटेड है और बाक़ायदा इनको संचालित करने के लिए इनके ठेकेदार होते हैं। उनका ये बहुत बड़ा कारोबार है।”
“क्या मतलब ?”n
“मतलब ये कि दिनभर भिखारी अपने प्राण होमकर जितना कमाते हैं, रात को जाकर अपने ठेकेदारों को सौंप देते हैं। इनकी मेहनत का कुछ भाग ही इन्हें नसीब होता है। जिस लड़की के लिए तुम उदास बैठी हो, क्या पता उसकी गोदी वाला बच्चा भी उसका न हो।”
महानगर की नब्ज़ बेटे ने कैसे और कब पकड़ ली? कहने को मैं भी बीसियों साल से इसी शहर में रहती आ रही हूँ फिर भी इससे अनभिज्ञ ही रह गयी । हाँ, ये हो सकता है कि मेरी पॉकेट ने मुझे बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं दी ।
“ये खुद से बतियाने का क्या सिस्टम है अम्मा आपका ?”
“तुम क्या कहते जा रहे हो केतन! मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।”
“अम्मा ये आपकी मर्जी…। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ।” उसने ये बात बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ कही थी। कुछ बेटे की रुखाई और कुछ महानगरीय कुत्सित भावना को सोच-सोचकर मेरी आँखें फ़ैलती चली जा रही थीं। मुँह का छाला कुछ ज्यादा ही टीसने लगा था। बचपन की वो बात- “सबसे भले भीख के रोट, कभी न आये तन पर चोट!” दिमाग़ में ठक-ठक बज उठी थी। उस बिना पर तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है । भीख माँग कर तन क्या, इनकी तो आत्मा तक घायल हुई जा रही है।
मुझे लगा एक साथ घंटनाद कर मेरे चारों ओर लोग करुण कथाएँ बाँचने लगे थे। छाती पर भारी बोझ सा आ गिरा था। कैसा है ये महानगर? यहाँ लड़कियाँ तो सुरक्षित नहीं, बूढ़े लोग तो नौकरों के हाथ लूट लिए जाते हैं और भिखारी औरों के लिए भीख माँगते हैं ? इससे तो अच्छा होता ये लोग अपने छोटे गाँव,कस्बे और शहर को छोड़ कर ज्यादा के फेर में पड़कर यहाँ आते ही नहीं। वहाँ रहकर जो जितना रूखा-सूखा कमाता पूरे स्वामी भाव से उसको अपनी पूँजी समझकर बरतता ।
मन की उथल-पुथल में लंबे रास्ते भी बौने लगने लगते हैं। हम कब दवा की दुकान के सामने तक जा पहुँचे, पता न चला। अब तक हमारे बीच हँसी-खुशी की सारी खबरें फुर्र हो चुकी थीं। जरूरत भर हम एक दूसरे से बोल रहे थे।
बेटे ने कहा, “अम्मा! तुम गाड़ी में बैठोगी या…?”
बिना बोले ही मैंने गाड़ी में बैठे रहने का इशारा कर दिया तो उसने गाड़ी के शीशे डाउन किए और ‘प्रिसक्रिप्शन’ लेकर चला गया।
पार्किंग में लगी गाड़ी के भीतर बैठना भी मेरे लिए एक कठिन काम था। रिक्शा पर बैठो तो चाहे वह चले या न चले, घुटन न होती थी। बीते दिन यादों के पानी से मन को किंछ गए। दिमाग़ बोरियत ओढ़ता उसके पहले मेरी नज़र टाइमपास जैसा कुछ ढूँढने लगी। देखा सड़क की दाहिनी ओर एक कतार में मेगामार्ट,सफ़ल और एक बेकरी शॉप रोशनी से सराबोर अपने आँचल में हजारों ख्वाहिशें पूरी करने की दमखम समेटे मचल रही थी। ‘रेड लाइट’ से ये वाला दृश्य बिल्कुल अलग लग रहा था। यहाँ बड़ी-बड़ी गाड़ियों से उतरने वाले खिले-खिले चेहरे न मेरी तरह छाले के दर्द में थे और न ही उस लालबत्ती वाली लड़की की तरह…।
वे तो धनतेरस को सच में धनतेरस का सुख देने आए थे। उसको चमकदार बनाने आये थे। तेरस धन की हो तो धनवान ही न उसका सुख लेगा। गरीब के पास न धन होता है और न तेरस वाला मन। “मंजुला! अब तो कोई नया तलाशो।” अपने आत्मबोध पर मैंने सिर झटक दिया।
सोचते हुए मैंने अपनी गर्दन बाईं ओर घुमाकर देखा। इस ओर फुटपाथ पर पेड़ों की घनी डालियों के गुम्फ़न के कारण सड़क पर अँधेरा पसरा था। लग रहा था मानो किसी आलीशान कोठी के पास फूंस की झोपड़ी सिर झुकाये, उजाले के बवंडर के बीच रहकर भी अपने हिस्से का उदास अँधेरा लीप रही थी। इसी विपर्यता को सम पर लाने के लिए हम दिन-रात दौड़ते रहते हैं। फ़िर भी स्थायी उजाले नहीं जुटा पाते। मैंने अकेलेपन का उपयोग करते हुए ज़ोर से बोला और ऊपर की ओर देखने लगी । पेड़ निर्विकार भाव में लीन थे । ऐसे तटस्थ मन हम मनुष्य को क्यों नहीं मिलते?
खैर, फुटपाथ पर देखा तो चार रेहड़ियाँ खड़ी थीं। उनमें से तीन पर सन्नाटे के बीच एक-एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी जो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त होने वाली थीं।लगता था इस ओर फुटपाथ की नीरसता ने उनके मालिकों को टिकने न दिया था लेकिन उन लोगों ने तीनों रेहड़ियों को एक साँकल से बाँध दिया था। एकता के इस रूप का मतलब रेहड़ियों का सुरक्षित बचे रहना था। छोटे दीये-सी खुशी मेरे होठों के भीतरी हिस्से पर तिर आई।
लगभग दो मिनट बाद मैंने अपने बालों को सम्हालते हुए कार के शीशे से उसी फुटपाथ के दूसरे कोने पर झाँका तो एक जोड़ा मार्ट से आने वाली धुँधली रोशनी में सुनहरी पन्नी से एक रेहड़ी को सजाने की जुगत में जुटा दिखाई पड़ा। बिकने के लिए चमकना कितना जरूरी है! मैं उन्हें और उनकी जुगत को ध्यान से देखने लगी और देखते-देखते रेहड़ी सजकर तैयार हो गयी। दोनों ने जल्दी से एक लंबे सरिये पर जो ऊपर से झुका था…दूधिया रोशनी छोड़ने वाली नन्हीं सी एल.ई.डी. जला दी। कचरे की बाल्टी में बची-खुची कतरन डालकर किनारे रख दी। कागज की प्लेटें,पानी का लाल कैम्पर, काठ की चम्मचें सही जगह पर रख दी गयी थीं। दो प्लास्टिक की चेयर रेहड़ी से हट कर डाल दी गईं फ़िर थोड़ी दूरी पर रखी बाल्टी से स्त्री ने पानी लेकर अपने हाथ मुँह धोये और छोटे से शीशे में खुद को देख, रेहड़ी के पास आकर भट्ठी के दो बार पाँव छू लिए। ये देखकर उसका आदमी मंद-मंद मूंछों में मुस्कुरा पड़ा। आदमी के सिर पर जमी धूल की परत रोशनी में दूर से दिख रही थी। स्त्री ने उसके अपनी ओर झुकाया और साड़ी के पल्ले से उसका सिर साफकर पल्ले को कमर में फेंटे की तरह कस लिया।
आदमी ने मद्धिम जलती अँगीठी पर बड़ा-सा चीकट तवा चढ़ा दिया और स्त्री लंबी-सी कलछुल से तवे पर टुनटुन करने लगी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का मन बहला रही हो। रेहड़ी वाली सारे हथकंडे आने-जाने वालों पर अपना रही थी लेकिन कोई उधर फटकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर में ही उनके उत्साह का गुब्बारा धीरे-धीरे पिचकने लगा था। सामने दुकानों की चहल-पहल देखकर वह अपने आदमी के कंधे के पास मुँह ले जाकर बुदबुदाई लेकिन वह कुछ कतरने में व्यस्त था,सो कुछ नहीं बोला। वह फिर रेहड़ी पर तुनक कर खड़ी हो गयी ।
दोनों की उदासी ओवरफ्लो होकर अब मेरे पास तक बह आयी थी। मुझे अपने बचपन के दिन अनायास याद आने लगे सो मैं उनकी गमगीनी में भीगती चली जा रही थी। गरीबी के बुखार की दवा आख़िर कब तक बन पाएगी? बरबस ही मेरा हाथ अपने माथे पर चला गया। देखा मन के साथ-साथ मेरा माथा भी गरम हो चला था| मैंने पीछे सीट का सहारा लेते हुए अपनी आँखें मिंची ही थीं कि एकाएक अतीत के पन्ने पलटते चले गये।
” अरी मेरी माँ! कहाँ है तू! जिंदगी बड़ी बोझिल है अब भी?”
“हाँ बोल न क्या हुआ रे?”
“माँ! तू सुन रही है न ?”
“हाँ भई बोलो तो !”
“तुझे गरीबी का अंकगणित लगाते-लगाते देख मैं आठवीं की परीक्षा दूँगी लेकिन तेरी गृहस्थी के सवाल हल न हुए! हज़ार जुगतों के बाद भी गरीबी का एक हाँसिल तेरे पास बच ही जाता है। मैं कुछ नहीं जानती इसबार दीवाली पर मुझे नई ड्रेस चाहिए ही चाहिए माँ।”
मैंने अपनी सहेली की नई फ्रॉक की हूक एक साँस में माँ के ऊपर उड़ेल दी और पाँव पटकने लगी।
“ये क्या कह दिया रे तू ने? तू तो मेरा समझदार बच्चा है।”
“आज नहीं हूँ ….।”
“न सुगंध ऐसे नहीं कहते। दिदिया के पुराने कुर्ते से एक बहुत अच्छी कुर्ती तेरे लिए आज ही सिली है। उसके आगे सबकी नई फ्रॉकें फेल हो जायेंगी।”
“झूठ, एकदम झूठ। मैं कुछ नहीं जानती। दिदिया के लिए फिर पीली साड़ी क्यों आई है?इसलिए मुझे भी चाहिए। जब देखो तब मेरे लिए कभी भाई के कपड़ों से कभी दिदिया की उतरन से गूँथन गूँथती रहती हो।”
“उससे होड़-हिर्स मत कर छोकरी। कुछ दिन की मेहमान बची है कुसुम। अच्छे से घर-वर मिल जाये,बस। अभी से न जोड़ें उसकी पहरावन ?”
“पट्टी पढ़ाने में एक नम्बर है तू माँ । ठीक है ठीक है। मुझे खाना दे।”
“तुझे अकेले क्या…? सब को बुला न।”
“आ जाओ सब लोग,भोजन तैयार है,माता ने बुलाया है।” सभी एक साथ जुट आये,दिदिया भी।
“माँ आज हम शक़्कर से रोटी खाएंगे ।” भाई ने कहा ।
“भाई खायेगा तो हम भी…।” मैंने भी कह दिया।
“क्यों? गुड़ काटता है तुम सबको? जो शक़्कर पर चढ़े रहते हो।”
“शक़्कर की वकालत करने पर माँ को इसबार सरकार इनाम देगी दिदिया।”
सभी फिक्क से हँस पड़े लेकिन दिदिया नहीं…। भाई ने फिर से कह दिया, “दे नss…।”
झुँझलाकर माँ बोली,” सुगंध ले आओ न अमरित!” फिर क्या शक़्कर की कत्थई बोतल दौड़ती हुई हमारे बीच आ गयी और भाई के साथ-साथ सबमें चुटकी-चुटकी बाँटी गयी।
“तू भी खाके देख न दिदिया बहुत मीठी है शक्कर और माँ तू भी। बहुत अच्छी लगती है शक़्कर से रोटी।” मैंने रोटी का टुकड़ा चुभलाते हुए कहा।
“हाँ हाँ पता है। जाकर रख आ।”
“तुझे मेरी कसम माँ! एक चुटकी खा बस्स।”
“महंगाई देखी है?” माँ बुदबुदाई होंठों में। फिर बोली “नहीं रे! तेरी दिदिया को ब्याहना है अबकी। शक्कर खायेंगे तो कैसे काम चलेगा।” अपने ब्याह की बात सुन दिदिया तो भाग गई लेकिन मैंने माँ से पूछा ।
“माँ, तू इतना अपने मन को क्यों मारती रहती है?”
“मरने के लिए,जा भाग जा यहाँ से ।”
“बोतल रखक कर लौटी तो देखा। गीली उँगली के सहारे ज़मीन पर छरके पड़े शक़्कर के दानों को उठा कर माँ अपने मुँह में डाल रही थी। रुको माँss मैं लाती हूँ शक्कर कहकर मैं उल्टे पाँव शक्कर लेने फिर दौड़ पड़ी।
तभी पीं पीं पीं करती हुई बगल से निकलने वाली गाड़ी ने तेज़ हॉर्न बजाया तो एक कौंध के साथ लगा कि सोते से जाग गई मैं। पलकें भारी हो चुकी थीं लेकिन निगाह उठी तो सीधे रेहड़ी पर फिर से जाकर गिरी।
वहाँ अब भी खामोशी का आलम था। दोनों के हावभाव में शिथिलता आती जा रही थी। दूधिया रोशनी मटमैली हो चली थी। उनके लटके चिंताग्रस्त निचुड़े चेहरे देखकर सोचा आस-पास निकलने वालों से चिल्ला-चिल्लाकर कहूँ,”मेरे मुँह में छाले हैं तुम लोग तो कुछ ख़रीदकर खा लो” लेकिन मन का सोचा भला कब किसने सुना है और भीख देकर उनके स्वाभिमान को मैं गिराना नहीं चाहती थी और न ही दान देकर उनकी कार्मिक उमंग को क्षति पहुंचाना चाहती थी। किसी के मन की उथल-पुथल यदि देख सुन ली जाती तो दुनिया का रंग ही कुछ और होता। सोचते हुए मैंने अपना पर्स थथोला और गुड़ी-मुड़ी पड़े सारे रुपयों को सीधे कर रख गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसकी ओर चलती चली गयी ।
पास में जाकर देखा तो दृश्य और भी झकझोरने वाला प्रतीत हो रहा था।
“क्या बना रहे हो भाई आप लोग?”
“चिकन टिक्का। खाइए न! बहुत स्वाद है इसमें। एक बार खाओगी तो बार-बार आओगी मैम साब!”
उसने बड़े विज्ञापनी लहज़े में ललक कर कहा था। “मेम साब ! बनाएँ क्या एक प्लेट?”
“अरे हाँ हाँ।” उससे बोलकर मैं सोच में पड़ गयी।” मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब क्या करूँ?” छाती के अंदरूनी भाग में जलन का एहसास हुआ।
“ब…न…दो।” मुँह से अस्फुट से आधे-अधूरे शब्द ही निकल सके थे कि अचानक एक आवारा कुत्ता मेरी ओर आते दिखा तो धुँधले पड़ते जा रहे विचारों में एक ताज़ा विचार कौंध गया। फिर ये भी लगा कि मनुष्यों के खाने वाली चीज़ को मैं कुत्ते को… लेकिन दूसरे पल ’जो हो सो हो’ वाले विचार ने कुछ जादू कर दिया और मेरे मुख से निकल पड़ा।
“अरे! मैं चिकन नहीं खाती तो क्या हुआ? ये तो जरूर खाता होगा ।”
“क्या मैडम सा…?”
“कुछ नहीं, आप बिना मसाले की दो प्लेट चिकन टिक्का बना दो प्लीज ।”
मेरा ऑर्डर सुनने के बाद भी वह मुझे हैरानी से देख रहा था लेकिन उसकी जनानी ने चेहरे पर आये पसीने को ब्लाउज की आस्तीन से चटपट पोंछा और टिक्का बनाने में जुट गयी। मेरे बार-बार पुचकारने से कुत्ता भी उधर ही रुक कर रेहड़ी सूँघने में व्यस्त बना रहा ।
मुश्किल से पाँच से दस मिनट लगे होंगे, उसने कहा। “लीजिये बन गया मेम साब ।” उसका आदमी दोनों हाथों में कागज़ की प्लेटें लिए मेरे सामने खड़ा था।
“कितना दाम हुआ ?”
“दो सौ रुपये ।”
“बिना मसाले के भी,दो सौ रुपये?”
“आप कहें तो डाल देता हूँ…।”
“न न रहने दो।” रुपये गिनकर उसको पकड़ा दिए । कुत्ते को फिर से पुचकारा तो वह दुम हिलाने लगा।
“आप बुरा न मानें, तो ये दोनों प्लेटें मैंने इसके लिए ही बनवाई हैं। क्या इसको परोस दोगे?” मैंने संकोच में बहुत धीरे से झिझकते हुए कहा ।
“हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तो बेचने से मतलब मैम जी चाहे कोई भी खाए।” कहते हुए उसने दोनो प्लेट उसके सामने परोस दीं। उन दोनों ने आँखों ही आँखों में कुछ कहा जिसे मैं नहीं समझ सकी लेकिन कुत्ते ने अपने प्राप्य को प्रेम से सूंघा, इधर-उधर देखा और आगे के पांव फैलाकर उनकी बनाई ‘डिश’ का स्वाद लेने लगा।
दो मिनट रुककर मैंने वहाँ देखा तो लगा समय के उस छोटे-से टुकड़े पर उजला संतोष छलक आया था। मैं गाड़ी की ओर मुड़ चली थी़। थोड़ी सी आगे निकली तो कान में आवाज़ पड़ी। “मुझे भी बना दो एक प्लेट।” किसी ने रेहड़ी वाली से कहा था। थोड़ा और चली तब तक बेटा भी दवाई लिए आता दिखा। दूर से उसे देखकर अच्छा लगा लेकिन बिना उसके लिए रुके मैं सीधे आकर गाड़ी में बैठ गई। बेटे का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह कुछ पूछना चाहता था़ मुझसे लेकिन न जाने क्यों चुप साध कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब हम दोनों अपने-अपने सफ़र में थे किन्तु मौन भाव से । हाँलाकि चारों ओर का त्योहारी मौसम शोर में डूबता जा रहा था लेकिन मेरे भीतर के गहरे सन्नाटे टूटकर कुछ नया रच रहे थे ।
गाड़ी थोड़ी दूर चलकर दूसरे रास्ते पर मुड़ चली थी। मन में आया कि बेटे से पूछें कि दवाई कितने की मिली है? उसने अपनी गैस की गोली ली या नहीं…? लेकिन एक शब्द तक न फूट सका। कुछ बातों को किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है शायद इसलिए बिना दवाई के मेरे छालों के दर्द में कुछ आराम-सा हो चला था। पर बेटे के मन का तापमान पकड़ में नहीं आ रहा था। बहुत सोचने के बाद भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो गाड़ी में एफ.एम.रेडियो के कान ऐंठ दिए। अचानक गाना बज उठा,”इत्ती-सी हँसी…, इत्ती-सी खुशी…इत्ता-सा टुकड़ा चाँद का..! मैंने कनखियों से देखा तो केतन के चेहरे पर हँसी तो नहीं लेकिन शांत सहजता पसरने लगी थी।
कल्पना मनोरमा
१५.११.२०२०
ई-मेल kalpanamanorama@gmail.com

यह भी पढ़ें ………
एक पाती भाई/बहन के नाम ( कल्पना मिश्रा बाजपेयी )
अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी- दिन भर का इंतजार
आपको कहानी “इत्ती सी खुशी” कैसी लगी ? अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराए | अगर आपको अटूट बंधन की रचनाएँ पसंद आती है तो कृपया साइट को सबस्क्राइब करें व अटूट बंधन फेसबुक पेज लाइक करें |





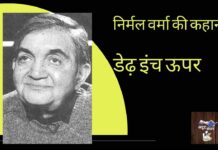
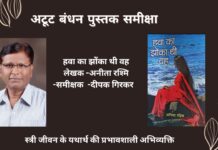

































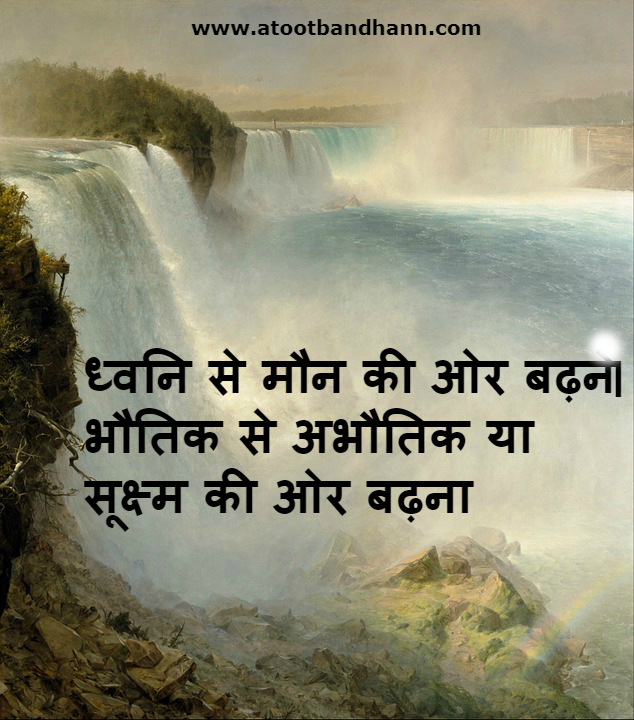






दिल को छू गई।बहुत सुन्दर